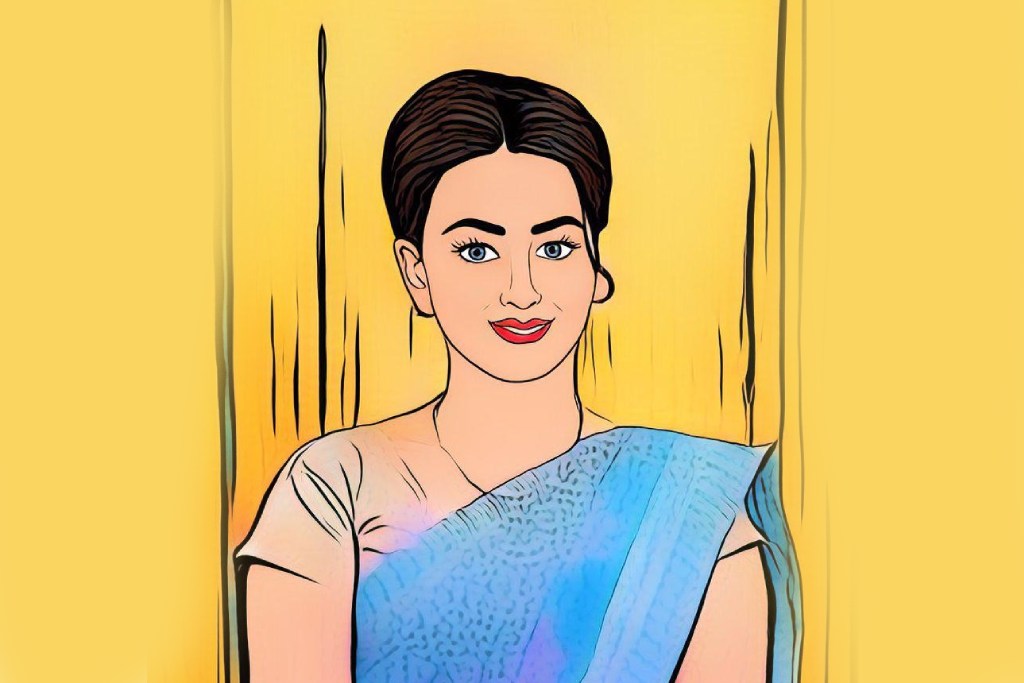ऑपरेशन की सफलता के पश्चात् उन्हें ऑपरेशन थियेटर से बाहर उनके निजी कमरे में लाया गया। तीनों पुत्रों के चेहरे खुशी से चमक उठे। ये माँ थी उनकी,जिसने वैधव्य के संघर्ष पूर्ण जीवन को जीकर आज उन्हें इस बड़े नगर के सर्वोत्तम अस्पताल में उनका उपचार करने के लायक बनाया था।
कुछ समय की अचेतावस्था के दौरान सुप्त पड़े उनके मस्तिष्क को अपने मंझले पुत्र के स्वरों से जागने का अहसास हुआ, ‘नहीं, बड़े भैया! माँ मेरे साथ ही जाएंगी।आप मुझ पर विश्वास करें।अब मैं आपका पहले वाला गैर जिम्मेदार ‘मंझला’ नहीं रहा। माँ की देखभाल के लिए अब मैं भी परिपक्व हो चुका हूँ। फिर, आप और छोटू दोनों हैं तो इसी नगर में न ! प्लीज,माँ को होश आने के पश्चात् हम इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करेंगे।’
मंझले के ‘अब मैं पहले वाला गैरजिम्मेदार मंझला नहीं रहा’ वाक्य से उनकी दाहिनी आंख की बाहरी कोर से निकली आंसुओं की धार ने उन्हें उनके अतीत में पहुंचा दिया।
विवाह के पश्चात आर्थिक रूप से अपने औसत स्तरीय परिवार में उनका वैवाहिक जीवन खूब मजे में चल रहा था। पति सामान्य आढ़त-व्यापारी थे। रईसी रहन-सहन तो नहीं था किंतु, किसी प्रकार की तंगी भी नहीं थी। पति केवल दसवीं पास थे,किंतु अति तीव्र बुद्धि से कारोबार कुशलता से चला रहे थे। उन्होंने दसवीं के पश्चात जे.बी.टी की टीचर ट्रेनिंग भी ली हुई थी।
हालांकि,अपनी इस अतिरिक्त योग्यता का वे एक समय तक उपयोग नहीं कर पाई थीं क्योंकि व्यापारिक मानसिकता वाले उनके इस घराने में स्त्रियों का नौकरी करना प्रतिष्ठा के विरुद्ध माना जाता था।
वैसे उन्होंने भी कभी इस विषय को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा था क्योंकि विवाह के प्रथम वर्ष में बड़े बेटे ने उनकी गोद भर दी थी और फिर उनका घर सदैव तीन वर्षीय ‘छोटू’ की किलकारियों, छः वर्षीय ‘मंझले’ की शैतानियों और दस वर्षीय ‘बड़े’ की मासूमियत भरी रौबदार आवाजों के साथ-साथ पति के उनके प्रति अतिशय प्रेम से भरा रहता था।
लेकिन भाग्य को कुछ और स्वीकार था। एक दिन प्रथम हृदयाघात में ही पति उन सबको रोता-बिलखता छोड़कर महाप्रयाण कर गए। वे विक्षिप्त-सी हो गईं। तेरह दिनों तक तो सगे-संबंधी आसपास रहे। लेकिन उनके चले जाने के पश्चात वे रोतीं तो उन्हें देखकर बच्चे भी बिलखने लगते।उन्होंने अपने आंसुओं को मन के एक कोने में कस कर बांध दिया,
जिन्हें वे अपने अकेले होने पर ही बहने की आज्ञा देतीं। फिर ,बड़ा बेटा माँ को सांत्वना देते-देते अपनी मासूमियत गंवाकर कब एकदम से ‘बड़ा’ हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला। ‘छोटू’ अभी नासमझ था। किंतु, नटखट तथा चुलबुला होने के कारण पापा का सर्वाधिक लाड़ला यह ‘मंझला’ तो पगला ही गया था। न खाना-पीना, न हँसना- खेलना, हर वक्त रो-रोकर बस एक ही रट कि ‘पापा पास जाऊँगा।
‘ घर की आर्थिक स्थिति से भी अब उनका आमना-सामना हुआ। उन्हें इस बात को समझने में देर न लगी कि जमा-पूंजी स्थिर होती है और घर चलाने के लिए धन की रवानगी जरूरी है।
अतः बड़े साहस के साथ उन्होंने अपने परिवार की रूढ़िवादी सोच को चुनौती देते हुए नगर के एक स्कूल में अध्यापिका के पद के लिए आवेदन दे दिया। उनके पिता की स्त्री-शिक्षा के प्रति जागृति सार्थक हुई और इस पद के लिए उनका चुनाव हो गया। उन्होंने नौकरी आरंभ कर दी। उनके द्वारा घर से बाहर निकल कर नौकरी करने से भी यह ‘मंझला’ ही अधिक प्रभावित हुआ
क्योंकि अपनी नौकरी के दौरान ‘छोटे’ को छोड़ने की व्यवस्था उन्होंने अपने स्कूल के निकट के ‘डे केयर’ में कर ली। वे आते समय उसे साथ ले आतीं और घर जाते समय साथ ले जातीं, किंतु, ‘मंझला’ पहले पिता का चले जाना और अब माँ का एक निश्चित समय के लिए घर से बाहर निकलना स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। धीरे-धीरे वह जिद्दी, चिड़चिड़ा, गुस्सैल, लापरवाह, गैर जिम्मेदार और विद्रोही बनता चला गया।
उसका सारा आक्रोश हमेशा उन पर ही निकलता और वे ममता की ढाल पर उसे झेल जातीं क्योंकि वे सब देख रही थीं, सब समझ रही थीं, लेकिन लाचार थीं। कभी-कभी अकेले में बैठकर रो भी लेतीं कि मेरे साथ-साथ यह भी मेरे वैधव्य की पीड़ा को झेल रहा है।
आखिरकार उनका संघर्ष रंग लाया। अपनी-अपनी शिक्षा के पश्चात ‘बड़े’ और ‘छोटू’ ने मिलकर पिता का कारोबार न केवल संभाला, अपितु आगे भी बढ़ाया, किंतु स्वभाव की विपरीतता के कारण यह ‘मंझला’ जीवन में एक बार फिर ठगा गया। उन दोनों के साथ अपना सामंजस्य न बिठा सकने से ‘बड़े’ ने पिता सम दायित्व निभाते हुए उसके लिए अलग घर और अलग आजीविका की व्यवस्था कर दी।
उनके द्वारा आपत्ति करने पर उसने उन्हें यह कहकर समझाया कि माँ इस प्रकार हम तीनों के परिवारों का प्रेम बना रहेगा। वैसे भी अपना यह पुश्तैनी घर छोटा है। अतः एक न एक दिन कोई विकल्प खोजना ही होगा। सो, समय रहते अभी क्यों नहीं। हमारा यह पग मंझले को जिम्मेदार बनाने में भी सहायक रहेगा।,लेकिन ,उनके बार-बार हठ करने पर भी उनका बड़ा बेटा अपनी माँ की संभाल
इस तथाकथित गुस्सैल एवं अक्खड़ बेटे को सौंपने को कदापि तैयार नहीं हुआ । उन्होंने परिस्थितियों के साथ समझौता अवश्य कर लिया, लेकिन अपने इस लाड़ले के बिगड़ैल हो जाने का ग़म उन्हें हमेशा सालता रहा।
ऑपरेशन थियेटर में जाते समय तो वे सोच रही थीं कि वे कितनी अभागिन हैं। इतने लंबे समय तक अपने वैधव्य के नासूर की जिस पीड़ा को वे अपने बच्चों से छिपाते हुए अपने अंदर ही अंदर दबाकर जीती रहीं,
आज संभवतः वही नासूर कैंसर के रूप में पुनः उभर आया है, किंतु अब ‘मंझले’ के स्वरों ने उनकी दबी हुई समस्त पीड़ा को अश्रुओं के रूप में बहाकर उन्हें पुनः सौभाग्य वान बना दिया था। बेटे’ का ‘प्रायश्चित’ उनके भावी सुकुन भरे जीवन के लिए बाहें पसारे खड़ा था।
तभी आंसुओं से गीले हो रहे तकिए की तरफ ध्यान जाते ही ‘मंझले’ की आवाज, ‘बड़े भैया.. छोटे, माँ को होश आ गया।’ से तीनों बेटे माँ के सिरहाने आ खड़े हुए।
उनके मुख पर अद्भुत मुस्कान आ गई । उन्हें लगा कि उनका सारा संघर्ष सफल हो गया है।
उमा महाजन
कपूरथला
पंजाब
साप्ताहिक विषय: प्रायश्चित