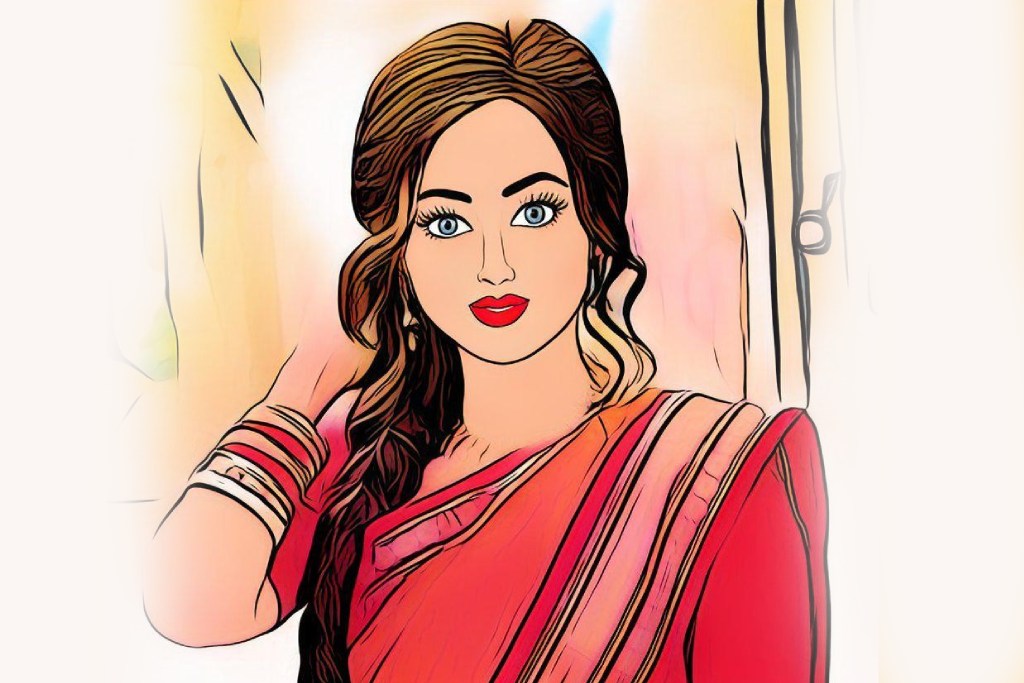गाँव की सीमा पर बिखरी झाड़ियों और सूखे पेड़ों के बीच एक टूटी-फूटी कोठरी में विश्वनाथ रहता था। उम्र के पचासवें पड़ाव पर खड़ा वह व्यक्ति, जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ नहीं, बल्कि उसके अंतस की उधेड़बुन दर्ज थी।
गाँव वाले उसे “पंडितजी” कहकर पुकारते, क्योंकि वह संस्कृत का विद्वान था और कभी मंदिर में पुरोहिती करता था। पर अब वह मंदिर के बजाय अपने अंधकारमय अतीत की गलियों में भटकता था।
एक दशक पहले की बात है। विश्वनाथ का बेटा, नीलकंठ, गाँव का पहला छात्र था जिसने शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति जीती। पर विश्वनाथ के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसकी यात्रा और रहने का खर्च उठा पाते।
तभी मंदिर के दान-पात्र में रखे चढ़ावे के पैसे उसकी नज़रों के सामने आए। एक रात, अंधेरे का लबादा ओढ़े, उसने ताला तोड़कर वह पैसे निकाल लिए। “कल सुबह लौटा दूँगा,” उसने स्वयं से कहा, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था।
उसी रात मंदिर में चोरी की खबर ने गाँव को हिला दिया। ग्रामीणों ने संदेह किया कि कोई बाहरी आया होगा। विश्वनाथ चुप रहा। नीलकंठ शहर चला गया, पर उसकी सफलता के हर पल में विश्वनाथ को लगता, जैसे मंदिर की मूर्तियाँ उसकी ओर तिरछी नज़रों से देख रही हों। समय बीता। नीलकंठ नौकरी पाकर गाँव लौटा, तो विश्वनाथ ने देखा—
उसका बेटा उसी मंदिर का जीर्णोद्धार करवा रहा था। नई मूर्तियाँ, सोने का कलश, चमकती दीवारें… पर विश्वनाथ के लिए वह मंदिर अब पूजा का नहीं, अपराध-बोध का स्थल था। एक दिन, जब नीलकंठ ने पूछा, “पिताजी, आप इतने उदास क्यों रहते हैं?” तो उसका गला रुँध गया। वह बोल नहीं पाया।
एक सर्द रात, जब चाँदनी ने धरती को चांदी के जाल में लपेटा था, विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में खड़ा था। उसकी आँखों के सामने वह दृश्य घूम गया—टूटा ताला, काँपते हाथ, और पैसों की गंध।
तभी उसने देखा, एक बूढ़ी औरत, जिसका बेटा बुखार से तप रहा था, मंदिर के दरवाज़े पर माथा टेककर रोने लगी, “हे भगवान, मेरे पास दवा के पैसे नहीं… कृपा करो।”
विश्वनाथ स्तब्ध रह गया। उस बुढ़िया की आवाज़ में वही करुणा थी, जो उस रात उसके अपने हृदय में दब गई थी। अचानक, उससे रहा नहीं गया। उसने अपनी सारी जमा-पूँजी—नीलकंठ द्वारा दिए गए पैसे, जो उसने कभी छुआ तक नहीं था—उस औरत के हाथ में रख दिए। “ले जाओ, तुम्हारे बेटे का इलाज होगा,
” उसने कहा, और फिर मंदिर की सीढ़ियों पर गिरकर फूट-फूटकर रो पड़ा। सुबह हुई, तो गाँव वाले हैरान रह गए। विश्वनाथ मंदिर के बाहर खड़ा था, और उसके गले में एक तख्ती लटकी थी, जिस पर लिखा था—”मैंने दस साल पहले इस मंदिर से पैसे चुराए थे। मेरी सजा शुरू होती है।”
लोगों ने उसे घेर लिया। कोई गुस्से में था, कोई हैरान। नीलकंठ ने आकर पूछा, “यह सब क्यों?” विश्वनाथ ने सच कह दिया। सुनकर नीलकंठ की आँखें नम हो गईं। उसने कहा, “पिताजी, आपने मुझे शिक्षा दी थी कि सच्चा जीवन वही है जो झूठ के बोझ से मुक्त हो। आज आपने मुझे सिखाया कि प्रायश्चित का अर्थ केवल पछतावा नहीं, बल्कि उस अंधेरे को स्वीकारना है जो हमारे भीतर घर कर जाता है।”
विश्वनाथ ने उस दिन से मंदिर की सफ़ाई शुरू की—बिना पैसे, बिना प्रसाद, केवल अपने पाप धोने की ललक में। गाँव वाले पहले तो उस पर हँसे, फिर धीरे-धीरे उसके साथ जुड़ने लगे। जिस मंदिर में उसने चोरी की थी, वहीं अब उसकी प्रार्थनाओं में एक नई आभा थी—निष्कलंक सच्चाई की। प्रायश्चित कोई घटना नहीं, एक यात्रा है—
अपने भीतर के उस ‘दूसरे’ से मुठभेड़, जो हमें हमारी नैतिक छाया दिखाता है। विश्वनाथ की कथा मनुष्य की उस शाश्वत पीड़ा का प्रतीक है, जहाँ पाप और पुण्य के बीच की रेखा इतनी धुँधली हो जाती है कि केवल आत्मा का आईना ही उसे साफ़ कर पाता है। सच्चा प्रायश्चित वह नहीं जो समाज के सामने किया जाए, बल्कि वह है जो उस अदृश्य देवता के सामने किया जाए, जो हमारे भीतर वास करता है।
डॉ० मनीषा भारद्वाज
ब्याड़ा (पालमपुर)
हिमाचल प्रदेश ।
Dr Manisha Bhardwaj