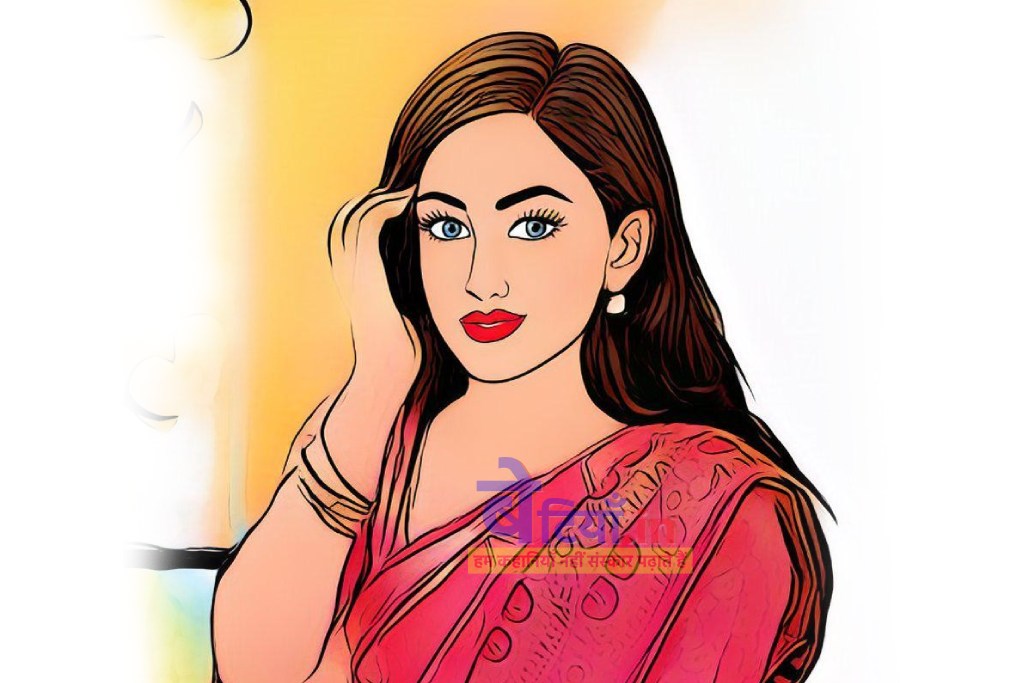उनका पांचवां पीरीयड फ्री था। वे स्टाफ रूम में पहुँची ही थीं कि चपड़ासी ने आकर सूचना दी कि एक महिला और एक युवक गैस्ट रूम में उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
वे गैस्ट रूम में आईं।महिला ने उठ कर उनका अभिवादन किया।युवक ने पूरा झुुुकते हुए उनके दोनों पांव छूकर कर उन्हें प्रणाम किया और हँसते हुए अत्यंत उत्साह से पूछा, ‘मैैडम ! पहचाना नहीं मुझे ?’ ‘अरे,नीरव तुम ! तुम्हें वाकई नहीं पहचान पाई, परंंतु तुम्हारी मां को पहचान लिया था।
तुम मिले भी तो लगभग 8-9 वर्ष बाद हो।क्या कर रहे हो आजकल ?’ ‘मैम ! एम.बी.करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ। एक प्रेजेंटेशन के सिलसिले में यहां आया था।सच कहूँ तो प्रजेंटेशन तो एक बहाना भर था ,असल में आपसे मिल कर,आपके हिंदी के पीरीयड मेें किए गए रीडिंग के अभ्यास का परिणाम आपको दिखाना चाहता था’ कहते-कहते नीरव खुल कर हँस पड़ा।
सुनने में काफी अजीब लगा कि कहां हिंदी की रीडिंग का अभ्यास और कहां एम. बी. ए.की पढ़ाई करके बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्य की उपलब्धि! परंतु सत्य तो यही था। वे आत्मविश्वास से लबालब नीरव को धाराप्रवाह बोलते सुनकर अद्भुत आनंद से भर उठी थीं।
नीरव ने उनके विद्यालय में नौवीं कक्षा में प्रवेश लिया था।वे उसकी कक्षा की इंचार्ज थीं और हिंदी विषय भी पढ़ाती थीं । सत्र प्रारंभ होते ही अपनी नई कक्षा में, शुरू के दो महीने तक, वे सप्ताह में दो दिन,केवल वाचन कार्य के लिए नियत रखा करती थीं। पंजाब के बच्चों को हिंदी पढ़ने-बोलने में निपुण बनाने का यह उनका अपना तरीका था।
कक्षा में वाचन के प्रथम दिवस जब अपनी बारी आने पर नीरव पढ़ने के लिए खड़ा हुआ तो सब बच्चे जोर-जोर से हँसने लगे। वे कुछ समझ पातीं कि इससे पूर्व ही एक छात्र स्वयं उठ खड़ा हुआ कि मैडम अब मेरी बारी है।नीरव नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि वह रुक-रुक कर बोलता है। पिछले स्कूल में भी उसकी बारी आने पर सब बच्चे हँसने लगते थे और वह बैठ जाया करता था।
इस कहानी को भी पढ़ें:
उन्होंने हँस रहे छात्रों पर एक तीव्र दृष्टि डालते हुए उस छात्र को बैठने का आदेश दिया और तुरंत नीरव की सीट तक पहुँचीं।नीरव शर्मिंदगी और डिगे हुए आत्मविश्वास से घबराया हुआ था। उन्होंने उसे पढ़ना शुरू करने को कहा।उसने डरते हुए उनकी ओर देखा तो उन्होंने उसकी पीठ सहलाते हुए अपने चेहरे की भाव- भंगिमाओं से उसमें आत्मविश्वास जगाने का प्रयास किया । वह धीरे-धीरे प्रयास करने लगा । उसके अटकने पर वे बार-बार उसकी सहायता करके हिम्मत बढ़ाती रहीं।उन्हें थोड़ा
सख्त देखकर बाकी बच्चे अब तक शांत हो चुके थे। एक-दो छात्रों ने तो नीरव के अटकने पर उसकी मदद करने का प्रयास भी किया । उस दिन का सारा वाचन नीरव ने ही किया । बीच-बीच में वे बाकी छात्रों को समझाती रहीं कि उन सबके हँसने से ही नीरव का आत्मविश्वास डोल चुका है। अब आप सबकी मदद से हमें उस आत्मविश्वास को वापिस लाना है।
नीरव की पारिवारिक पृष्ठभूमि जानने की दृष्टि से उन्होंने उसके माता-पिता को विशेष रूप से स्कूल में बुलवाया था, लेकिन उसकी मां अकेली ही आई थीं। उसके पिता नहीं आए थे और तभी उनके समक्ष न केवल नीरव, अपितु उसकी मां के मन की भी अनेक गांठें खुली थीं।
मां ने रोते हुए बताया था कि नीरव पहले ऐसा नहीं था। उसे वाणी संबंधी कोई गंभीर रोग भी नहीं है। परंतु वह बचपन से ही अपने पिता के अत्यधिक क्रोधित स्वभाव के कारण घर में बहुत डरा- डरा रहता था। प्रकृति वश ,उनकी बड़ी बेटी पढ़ाई में काफी होशियार है,किंतु नीरव औसत स्तर का है।
इस अंतर के कारण नीरव पिता के प्रेम से वंचित होता जा रहा है। उसके ‘सहम’ ने धीरे-धीरे उसके मन में ‘हीन भावना’ की एक मजबूत गांठ बना ली है जो अब उसकी ‘हिचकिचाहट’ और ‘हकलाहट’ में उभरने लगी है। पति के अत्यधिक क्रोध से वे स्वयं भी पीड़ित रहती हैं और भय के कारण नीरव को,पति के हिस्से का तो क्या, अपने हिस्से का स्नेह व दुलार भी नहीं दे पाती हैं।अब तो वह घर से बाहर,आस-पड़ोस और स्कूल में भी गुमसुम रहने लगा है।
इस मुलाक़ात से वे समझ गई थीं कि नीरव सिर्फ ‘उपेक्षा’ का शिकार है। पिता के आतंक ने उसे ‘दब्बू’ बना दिया है और इसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव उसकी वाणी पर पड़ा है। उन्होंने मन ही मन, उपेक्षित होते जा रहे नीरव को अतिरिक्त स्नेह के बल पर सामान्य बालकों के समान वाक् पटु बनाने की चुनौती को स्वीकार कर लिया था।
इस कहानी को भी पढ़ें:
प्रतिदिन किए जाने वाले कक्षा अभ्यास और बाकी छात्रों के सहयोग से धीरे-धीरे नीरव का मनोबल बढ़ता गया।उन्हें याद है कि नीरव के इस वाक्-दोष ने ही उन्हें अपनी कक्षा में दैनिक जीवन के सामान्य विषयों पर केवल 1 से 1.30 मिनट की चर्चाएं और आशु भाषण करवाने का विचार दिया था।नौंवी कक्षा में भी रोटी,दूध,सब्जी,यूनिफॉर्म, बूट, चप्पल बहन,मां,पिता,रसोईघर जैसे सरल-साधारण विषयों पर चर्चा का सभी छात्र खूब आनंद उठाते थे। नीरव को बोलने के अधिक से अधिक अवसर देकर अन्य छात्रों द्वारा दिए जाने वाले सहयोग को वे भली भाँति देख पा रही थीं।
धीरे-धीरे छात्रों के सहयोग से किया गया उनका प्रयास अपना रंग दिखाने लगा था।नीरव न केवल ठीक से बोलने लगा था अपितु बोलने के लिए उत्सुक और उत्साहित रहने लगा। एक दिन स्टाफ रुम में जब उन्होंने अंग्रेजी और पंजाबी की अध्यापिका को भी नीरव में आ रहे इस परिवर्तन के संबंध में बातचीत करते सुना तो वे भाव विभोर हो उठी थीं।
नीरव की मां ने भी एक ‘पेरेंट्स मीटिंग’ के दौरान उन्हें व्यक्तिगत रूप से बताया था कि नीरव का जगा आत्मविश्वास अब उसे अपने पिता के आतंक का सामना करने में भी सहायक होने लगा है। इस बात को बताते हुए मां की आँखों में आई अनोखी चमक पर वे बरबस मुस्कुरा उठी थीं।
नौंवी तथा दसवीं पास करने के पश्चात नीरव ने कॉलेज का रुख कर लिया था और उनका उससे पुनः संपर्क नहीं हो पाया था, किंतु आज एक ‘अलग’ ही नीरव उनके समक्ष खड़ा था। कहां वह हकलाता हुआ, डरा-सहमा, दबा-दबा सा बालक नीरव और कहां यह पूर्ण आत्मविश्वास से सुसज्जित धाराप्रवाह बोलता सुदृढ़ युवक नीरव !
सहसा नीरव की मां की आवाज ने उन्हें चौंकाया, ‘मैम, क्या सोचने लगीं आप ? आज मैं भी आपके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए ही नीरव के साथ आई हूँ।आपने एक चिकित्सक की भाँति नीरव के वाणी दोष को दूर करके एक मां को भी नवजीवन प्रदान किया है।’
और वे नीरव एवं उसकी मां के चेहरे की दीप्ति को अपलक निहारते हुए आज अपनी इस स्वयं-स्वीकृत चुनौती की सफलता पर अभिभूत हो उठी थीं ।
उमा महाजन
कपूरथला
पंजाब।