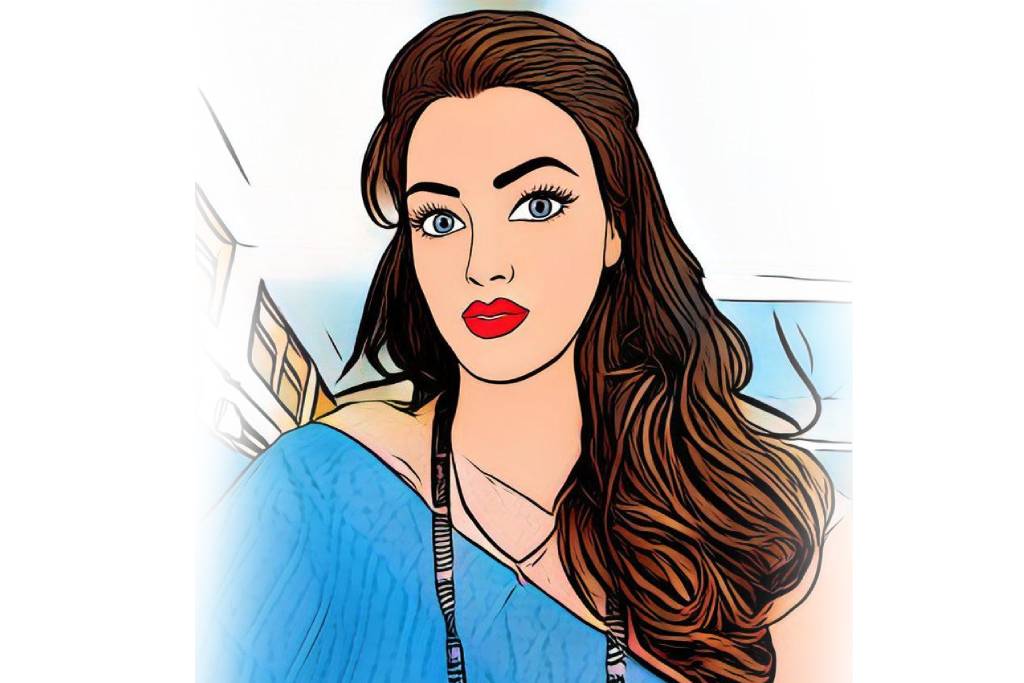बैंड-बाजे के शोर में सुमिता जब ससुराल पहुँची, तो दरवाज़े पर उसकी अगवानी के लिए पूरा परिवार खड़ा था। आरती का थाल, फूलों की वर्षा, ढोल-नगाड़े… और सासू माँ का भावुक बयान—
“अब ये घर तेरा ही है, बेटी!”
लेकिन सुमिता को जल्दी ही समझ आ गया कि ‘तेरा ही है’ का असली मतलब यह था कि घर में हक़ से झाड़ू लगा सकती हो, रसोई संभाल सकती हो और सबकी पसंद का खाना बना सकती हो, लेकिन सोफे पर पैर रखकर बैठने की आज़ादी नहीं है!”
शाम की चाय जब भी बनती, सासू माँ बड़े प्यार से कहतीं—”बहू, चाय बनाते समय याद रखना, पहले दूध को उबाल लो, फिर पत्ती डालना। और हाँ, चाय को तेज़ मत करना, वरना घर के संस्कारों की तरह इसका स्वाद भी बिगड़ जाता है!”
“अब चाय बनाने में भी संस्कार घुलने लगे हैं,, मगर क्या करें, यहाँ की चाय भी ठहरी संस्कारी!” सोचकर सुमिता मुस्कुरा देती।
सुबह जल्दी उठने का नियम था, लेकिन उसे कोई नहीं बताता था कि सासू माँ का मतलब ‘जल्दी’ से क्या था। वो छह बजे उठी, तो ताना मिला—”बहू, हमें तो पाँच बजे की आदत है!” अगली सुबह पाँच बजे उठी, तो सुनने को मिला—”अरे, इतनी जल्दी? पहले थोड़ा आराम कर लेती!”
टीवी पर धारावाहिक चल रहा होता, और सुमिता जैसे ही रिमोट उठाती, उसकी सास को “इसी वक्त” धार्मिक प्रवचन देखने का मन होने लगता। चाय कैसी बनेगी, कितनी बार बनेगी, कौन-सी दाल पसंद की जाएगी—सबका संविधान पहले से तय था। और तो और, यहाँ तक कि रात को सोने के लिए तकिया किस तरफ रखना है, इसका भी नियम था!
इस कहानी को भी पढ़ें:
शुरू-शुरू में उसने सोचा, “अभी नई हूँ, धीरे-धीरे सब अपने आप ठीक हो जाएगा।” लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि इस घर में चीज़ें ‘अपने आप’ नहीं होतीं। जब उसे महसूस हुआ कि उसे सिर्फ ‘करने’ की छूट है, पर ‘फैसले’ का नहीं, तो उसका धैर्य जवाब देने लगा।
एक दिन सासू माँ ने घोषणा की—”आज मूंग की दाल की खिचड़ी बनेगी। हमारे यहाँ हमेशा यही बनती है!”
सुमिता चुप रही, लेकिन उसके अंदर हलचल मची थी। उसने हिम्मत जुटाई—”माँजी, क्या मैं अरहर दाल की खिचड़ी बना सकती हूँ?”
घर में सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा, जैसे किसी ने किसी पुराने महल की दीवार में सेंध लगाने की कोशिश की हो। ससुरजी ने अख़बार से झाँककर देखा, देवर ने मोबाइल से ईयरफोन निकाल दिया, पति ने चाय का कप नीचे रख दिया। सासू माँ की आँखों में वही भाव था, जो रेलवे स्टेशन पर गाड़ी छूटने के बाद यात्री के चेहरे पर आता है।
“हमारे यहाँ मूंग की ही खिचड़ी बनती है, बेटा। ये तो परंपरा है!”
सुमिता के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। “तो अब दाल भी खानदानी हो गई?” उसने मन ही मन सोचा, लेकिन कुछ बोली नहीं।
“घर बदल जाता है, पर क्या बहू का हक भी बदल जाता है?” यही सवाल सुमिता के मन में अक्सर उठता। शादी को छह महीने हो चुके थे, मगर उसे अभी तक ससुराल में अपनी ‘जगह’ का एहसास नहीं हुआ था। यह सिर्फ चार दीवारों का सवाल नहीं था, बल्कि उसके अधिकारों, उसकी पहचान और उसकी अहमियत का भी सवाल था।
अगले दिन उसने बिना कुछ कहे चुपचाप अरहर की दाल की खिचड़ी बना डाली। जब थाली परोसी गई, तो सासू माँ ने नाराज़गी दिखाते हुए पहला कौर लिया और तुरंत बोल उठीं—”अरे! नमक थोड़ा कम होता तो और अच्छा होता!”
सुमिता जान गई कि यह ‘अस्वीकृति’ नहीं, बल्कि ‘स्वीकृति’ थी और इसी के साथ, क्रांति की पहली जीत दर्ज हुई।
एक शाम अचानक गोलगप्पे खाने की तलब हुई। जैसे ही वह बाहर जाने के लिए निकली, सासू माँ की आवाज़ आई—
अकेले बाहर? हमारे घर की बहुएँ यूँ सड़क पर गोलगप्पे नहीं खातीं!”
इस कहानी को भी पढ़ें:
अब सुमिता के दिमाग़ में झाँसी की रानी वाला विद्रोही भाव जागा—”गोलगप्पे खाने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ेगी?”
उसने मुस्कुराकर कहा—”ठीक है माँ, तो आज घर में ही गोलगप्पे बनाएंगे!”
हमेशा तटस्थ की भूमिका निभाने वाले पति ने उत्साह में तालियाँ बजा दीं—”वाह! अब तो ससुराल भी गोलगप्पों के स्वाद से भीग जाएगा!”
सासू माँ पहले घूरने लगीं, फिर धीरे से बोलीं—”खट्टी चटनी सही बनाना!”
रात होते-होते सासू माँ भी गोलगप्पे खाते-खाते मज़े लेने लगीं। उस दिन सुमिता को एहसास हुआ कि कुछ हक़ लड़े नहीं जाते, धीरे-धीरे घोलकर पिलाए जाते हैं—जैसे चाय में चीनी! और फिर, ससुराल के इतिहास में पहली बार, गोलगप्पों का पर्व मनाया गया।
गोलगप्पों की सफलता के बाद, अगला मिशन था टीवी का रिमोट!
अक्सर सासू माँ सास-बहू वाले धारावाहिक देखती, जिनमें बहुएँ हमेशा रोती रहतीं और सासें साज़िशें रचतीं।
एक दिन जब सासू माँ किसी से बात करने में व्यस्त थीं, सुमिता ने झटपट रिमोट उठाकर खेल चैनल लगा दिया, जिस पर जिम्नास्ट अपने करतब दिखा रहे थे।सासू माँ किचन से बाहर आईं और जैसे ही टीवी स्क्रीन पर जिम्नास्ट को देखा, उनकी आँखों में वही भाव आ गया, जो किसी को ATM से 500 का नोट निकलने के बदले 100 का नोट निकल जाने पर आता है!
“बहू, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता!”
सुमिता मुस्कुराकर बोली—”माँ, कभी-कभी बदलाव भी अच्छा होता है। देखिए ये जिम्नास्ट कितना फ्लेक्सीबल है, जिन्दगी भी ऐसी ही होनी चाहिए, है ना माँ!” बोलकर सुमिता झट से रसोई में घुस गई और वहाँ से देखा तो सासू माँ किसी विचार में खोई हुईं थीं।
अब सासू माँ के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उस दिन से घर में कभी क्रिकेट, कभी सीरियल और कभी-कभी धार्मिक प्रवचन भी आने लगा।]
इस कहानी को भी पढ़ें:
धीरे-धीरे, चीज़ें बदलने लगीं।
अब सासू माँ पूछने लगीं—”बहू, आज क्या बनाने का मन है?”
पति मुस्कुराते हुए बोले—”माँ, अब इस घर में दो तरह की खिचड़ी चलेगी—मूंग की भी और अरहर की भी!”
सासू माँ ने हँसते हुए कहा—”ठीक है, लेकिन गोलगप्पे बनाना मत भूलना!”
उस दिन सुमिता को एहसास हुआ कि ससुराल में हक़ लड़कर नहीं, प्यार से लिया जाता है—जैसे गोलगप्पों में पानी धीरे-धीरे भरा जाता है! कुछ लड़ाइयाँ चिल्लाकर नहीं, धीरे-धीरे मुस्कुराहटों से जीती जाती हैं। सुमिता को अपने हक़ की लड़ाई जीतने के लिए कोई बगावत नहीं करनी पड़ी, बस उसने धीरे-धीरे अपने होने का एहसास करवाया। अब यह घर सिर्फ उसका ‘कर्तव्य’ नहीं, उसका ‘हक’ भी बन चुका था!
✍️आरती झा आद्या
दिल्ली
#ससुराल में हक